 हमारे चारो तरफ आग लगी है. सीमाएं सुलग रही हैं – चीन से मिलने वाली भी और नेपाल से मिलने वाली भी ! पाकिस्तान से मिलने वाली सीमा की चर्चा क्या करें; उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है. बांग्लादेश, लंका और बर्मा से लगने वाली सीमाएं खामोश हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ कहना नहीं है बल्कि इसलिए कि वे कहने का मौका देख रही हैं. कोरोना ने सीमाओं की सीमा भी तो बता दी है न ! ताजा लपट लद्दाख की गलवान घाटी में दहकी है जिसमें सीधी मुठभेड़ में अब तक की सूचना के मुताबिक 20 भारतीय और 43 चीनी फौजी मारे गये हैं. 1962 के बाद भारत-चीन के बीच यह सबसे बड़ी मुठभेड़ है. सरकार इसे छिपाती हुए पकड़ी गई है. चीन को अपने पाले में लाने की उसकी तमाम तमाम कोशिशों के बावजूद आज चीन सबसे हमलावर मुद्रा में है. डोकलाम से शुरू हुआ हमला आज गलवान की घाटी तक पहुंचा है और यही चीनी बुखार है जो नेपाल को भी चढ़ा है. कहा तो जा रहा था कि चीनी-भारतीय फौजी अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है जबकि सच यह है कि हम कहे जा रहे थे और वे सुन रहे थे. युद्ध की भाषा में इसे वक्त को अपने पक्ष में करना कहते हैं. चीन ने वही किया है.
हमारे चारो तरफ आग लगी है. सीमाएं सुलग रही हैं – चीन से मिलने वाली भी और नेपाल से मिलने वाली भी ! पाकिस्तान से मिलने वाली सीमा की चर्चा क्या करें; उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है. बांग्लादेश, लंका और बर्मा से लगने वाली सीमाएं खामोश हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ कहना नहीं है बल्कि इसलिए कि वे कहने का मौका देख रही हैं. कोरोना ने सीमाओं की सीमा भी तो बता दी है न ! ताजा लपट लद्दाख की गलवान घाटी में दहकी है जिसमें सीधी मुठभेड़ में अब तक की सूचना के मुताबिक 20 भारतीय और 43 चीनी फौजी मारे गये हैं. 1962 के बाद भारत-चीन के बीच यह सबसे बड़ी मुठभेड़ है. सरकार इसे छिपाती हुए पकड़ी गई है. चीन को अपने पाले में लाने की उसकी तमाम तमाम कोशिशों के बावजूद आज चीन सबसे हमलावर मुद्रा में है. डोकलाम से शुरू हुआ हमला आज गलवान की घाटी तक पहुंचा है और यही चीनी बुखार है जो नेपाल को भी चढ़ा है. कहा तो जा रहा था कि चीनी-भारतीय फौजी अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है जबकि सच यह है कि हम कहे जा रहे थे और वे सुन रहे थे. युद्ध की भाषा में इसे वक्त को अपने पक्ष में करना कहते हैं. चीन ने वही किया है.
देश के संदर्भ में सीमाओं का मतलब होता है संबंध ! इसलिए अमरीका से हमारे संबंध कैसे हैं या फ्रांस से कैसे हैं इसका जायजा जब भी लेंगे हम तब यह जरूर ध्यान में रखेंगे कि इनके साथ हमारी भौगोलिक सीमाएं नहीं मिलती हैं. सीमाओं का मिलना यानी रोज-रोज का रिश्ता; तो मतलब हुआ रोज-रोज की बदनीयती भी, बदमजगी भी और बदजबानी भी ! और रोज-रोज का यह संबंध यदि फौज-पुलिस द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है तब तो बात बिगड़नी ही है. इसलिए जरूरी होता है कि राजनयिक स्तर पर संवाद बराबर बना रहे और शीर्ष का नेतृत्व गांठें खोलता रहे. यह बच्चों का खेल नहीं है, मनोरंजन या जय-जयकार का आयोजन भी नहीं है. अपनी बौनी छवि को अंतरराष्ट्रीय बनाने की ललक इसमें काम नहीं आती है. सीमा का सवाल आते ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यह सबसे ह्रदयहीन चेहरा सामने आता है जहां सब कुछ स्वार्थ की तुला पर ही तौला जाता है. 1962 में यही पाठ जवाहरलाल नेहरू को चीन से सीखना पड़ा था और आज 2020 में नरेंद्र मोदी भी उसी मुकाम पर पहुंचते लग रहे हैं. इतिहास की चक्की बहुत बारीक पीसती है.
चीन का मामला एकदम ही अलग है. हमारे लिए यह मामला दूध का जला छांछ भी फूंक-फूंक कर पीता है, जैसा है. हम ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ के दौर से चल कर 1962 के युद्ध और उसमें मिली शर्मनाक पराजय तक पहुंचे हैं. हमारी धरती उसके चंगुल में है. चीन सीमा-विस्तार के दर्शन में मानने वाला और एशियाई प्रभुता की ताकत पर विश्वशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पालने वाला देश है. हमारे और उसके बीच सीमा का लंबा विवादास्पद भू-भाग है, हमारे क्षेत्रीय, एशियाई और अंतरराष्ट्रीय हित अक्सर टकराते दिखाई देते हैं. हममें से कोई भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, उसकी अंतरराष्ट्रीय हैसियत बड़ी हो तो दूसरे को परेशानी होती है. यह सिर्फ चीन के लिए सही नहीं है, हमारे यहां भी ऐसी ‘ बचकानी’ अंतरराष्ट्रीय समझ रखने वाले लोग सरकार में भी हैं और तथाकथित शोध-संस्थानों में भी. इसलिए चीन की बात जब भी हमारे बीच चलती है, आप चाहें, न चाहें इतनी सारी बातें उसमें सिमट आती हैं.
क्या मोदी सरकार ने इन सारी बातों को भुला कर चीन से रिश्ता बनाने की कोशिश की थी ? नहीं, उसने यह सब जानते हुए भी चीन को साथ लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था. दुनिया हमारे जैसी बन जाए तब हम अपनी तरह से अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है. दुनिया जैसी है उसमें ही हम अपना हित कैसे साध सकते हैं, यह देखना और करना ही सफल डिप्लोमेसी होती है. इसलिए इतिहास को बार-बार पढ़ना भी पड़ता है और उससे सीखना भी पड़ता है. हम चाहें, न चाहें इतिहास की सच्चाई यह है कि भारत-चीन के बीच का आधुनिक इतिहास जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है. इस सरकार की दिक्कत यह है कि यह इतिहास पढ़ती नहीं है और जवाहरलाल नेहरू से बिदकती है. इतिहास से ऐसा रिश्ता आत्मघाती होता है.
आजादी के बाद दो बेहद आक्रामक व क्रूर गुटों में बंटी दुनिया में नव स्वतंत्र भारत की जगह व भारत की भूमिका तलाशने का काम जिस जवाहरलाल नेहरू के सर आया था, उनकी दिक्कत कुछ अलग तरह की थी. उनके पास गांधी से मिले सपनों की आधी-अधूरी तस्वीर तो थी लेकिन तलत महमूद के गाए उस गाने की तरह “तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी’ का कठोर अहसास भी था. गांधी का रास्ता उनके दिमाग में बैठता नहीं था क्योंकि गांधी और उनका रास्ता, दोनों ही खतरनाक हद तक मौलिक था. उसे छूने के लिए बला का साहसी और आत्मविश्वासी होना जरूरी था. जवाहरलाल ने आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त ही इस गांधी को पहचान लिया था और उनसे अपनी दूरी तय कर ली थी. लेकिन यह सच भी वे जानते थे कि भारत की किसी भी नई भूमिका की परिपूर्ण तस्वीर तो इसी बूढ़े के पास मिलती है. इसलिए उन्होंने अपना एक आधा-अधूरा गांधी गढ़ लिया था लेकिन उसके साथ चलने के रास्ते उन्होंने अपने खोजे थे. ऐसा करना भी एक बड़ा काम था. अमरीकी व रूसी खेमे से बाहर तटस्थ राष्ट्रों के एक तीसरे खेमे की परिकल्पना करना और फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रयोग करना जवाहरलाल से कमतर किसी व्यक्ति के बूते का था ही नहीं. वे थे तो यह प्रयोग परवान चढ़ा. कई देशों को उन्होंने इसके साथ जोड़ा भी.
नहीं जुड़ा तो चीन. जवाहरलाल की विदेश-नीति के कई आधारों में एक आधार यह भी था कि एशिया के मामलों से अमरीका व रूस को किसी भी तरह दूर रखना. वे जान रहे थे कि ऐसा करना हो तो चीन को साथ लेना जरूरी है. लाचारी के इस ठोस अहसास के साथ उन्होंने चीन के साथ रिश्ते बुनने शुरू किए. वे चीन को, माओ-त्से-दुंग को और साम्यवादी खाल में छिपी चीनी नेतृत्व की पूंजीवादी मंशा को अच्छी तरह जानते थे. चीनी ईमानदारी व सदाशयता पर उनका भी भरोसा नहीं था. लेकिन वे जानते थे कि अंतरराष्ट्रीय प्रयोगों में मनचाही स्थितियां कभी, किसी को नहीं मिलती हैं. यहां जो पत्ते हैं आपके हाथ में उनसे ही औपको खेलना पड़ता है. इसलिए चीन के साथ कई स्तरों पर रिश्ते बनाए और चलाए उन्होंने. पंचशील उसमें से ही निकला. बात कुछ दूर पटरी पर चली भी लेकिन चूक यह हुई कि रिश्ते एकतरफा नहीं होते हैं सामने वाले को अनुकूल बनाना आपकी हसरत होती है, अनुकूलता बन रही है या नहीं, यह भांपना आपकी जरूरत होती है. चीन को भारत का वह कद पच नहीं रहा था. एशियाई महाशक्ति की अपनी तस्वीर के फ्रेम में उसे भारत कदापि नहीं चाहिए था. उसने तरह-तरह की परेशानियां पैदा कीं. नेहरू-विरोध का जो चश्मा आज सरकार ने पहन और पहना रखा है उसे उतार कर वह देखेगी तो पाएगी कि यह सरकार ठीक उसी रास्ते पर चल रही है जो जवाहरलाल ने बनाया था. फर्क इतना ही है कि वह नवजात हिंदुस्तान था, युद्ध व शीतयुद्ध से घिरा हुआ और तटस्थता की अपनी नई भूमिका के कारण अकेला पड़ा हुआ सारी शंकाओं व सावधानी के साथ उसे चीन को साथ ले कर इस स्थिति का समाना भी करना था और भारत की एक नई भूमिका स्थापित भी करनी थी; और आज जो हिंदुस्तान हमारे सामने है वह आजादी के बाद के 70 से अधिक सालों की बुनियाद पर खड़ा हिंदु्स्तान है. इसके सामने एक अलग ही दुनिया है. इस सरकार के पास न तटस्थता जैसा कोई सपना है, न पंचशील जैसी कोई अवधारणा. सत्ताधीश सरकारें ऐसे सपने वगैरह पालती भी नहीं हैं. यह वह दौर है जब अमरीका, रूस और चीन तीनों की अंतरराष्ट्रीय भूमिका सिकुड़ती जा रही है. चीन को साबरमती नदी किनारे झूला झुला कर, और अमरीका को ‘दुनिया’ के सबसे बड़े स्टेडियम में खेल खिला कर हमने देख लिया है कि नेहरू को 1962 मिला था, हमें 2020 मिला है. सीमा पर लहकती आग के साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम करीब-करीब अकेले हैं. यह 2020 का 1962 है. अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यह असली चेहरा है. लेकिन क्या कीजिएगा, रास्ता तो इसी में से खोजना है. तो यह सरकार भी रास्ता खोजे लेकिन इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को खारिज करने की नहीं, उनका रास्ता समझने की जरूरत है.
(16.06.2020)
My Blog : http://kumarprashantg.blogspot.in/
![]()
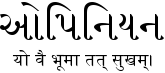

 पूरा देश तालाबंदी में गया तो जैसे कोई एक ताला खुला ही रह गया. नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान के बंद द्वार में बंद हुआ मैं देखता रहा सामने की सूनी पड़ी सड़क पर वह अबाध मानव-झुंड जो अपना पूरा अस्तित्व संभाले चल रहा था- लगातार-लगातार ! कोरोना से डरी नगरीय सभ्यता ने उनके मुंह पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे. वे सब जा रहे थे – भाग या दौड़ नहीं रहे थे, बस जा रहे थे. मैं जब-जब उन्हें देखता, मन कहीं दौड़ कर ‘पान सिंह तोमर’ के पास पहुंच जाता था ! यह फिल्म देखी है आपने ? मैंने जब से देखी तब से आज तक वैसी दौड़ दोबारा देख नहीं पाया हूं. इरफान उस फिल्म में बहुत कुछ कर गये हैं लेकिन जिस तरह दौड़ गये वह भारतीय सिनेमा का एक मानक है. ये अनगिनत और अनचाहे दिहाड़ी मजदूर, जो पता नहीं देश के किस कोने से निकले थे और पहुंचे थे अपनी राजधानी दिल्ली- और बिना स्वागत, बिना आवाज, बिना सूचना उन्होंने राजधानी का सारा कल्मष खुद पर ओढ़ लिया. मुझे खूब पता है कि उनमें से किसी ने भी दिल्ली की राजधानी वाला चेहरा देखा भी नहीं होगा, उनके लिए दिल्ली का चेहरा रोटी का चेहरा था.
पूरा देश तालाबंदी में गया तो जैसे कोई एक ताला खुला ही रह गया. नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान के बंद द्वार में बंद हुआ मैं देखता रहा सामने की सूनी पड़ी सड़क पर वह अबाध मानव-झुंड जो अपना पूरा अस्तित्व संभाले चल रहा था- लगातार-लगातार ! कोरोना से डरी नगरीय सभ्यता ने उनके मुंह पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे. वे सब जा रहे थे – भाग या दौड़ नहीं रहे थे, बस जा रहे थे. मैं जब-जब उन्हें देखता, मन कहीं दौड़ कर ‘पान सिंह तोमर’ के पास पहुंच जाता था ! यह फिल्म देखी है आपने ? मैंने जब से देखी तब से आज तक वैसी दौड़ दोबारा देख नहीं पाया हूं. इरफान उस फिल्म में बहुत कुछ कर गये हैं लेकिन जिस तरह दौड़ गये वह भारतीय सिनेमा का एक मानक है. ये अनगिनत और अनचाहे दिहाड़ी मजदूर, जो पता नहीं देश के किस कोने से निकले थे और पहुंचे थे अपनी राजधानी दिल्ली- और बिना स्वागत, बिना आवाज, बिना सूचना उन्होंने राजधानी का सारा कल्मष खुद पर ओढ़ लिया. मुझे खूब पता है कि उनमें से किसी ने भी दिल्ली की राजधानी वाला चेहरा देखा भी नहीं होगा, उनके लिए दिल्ली का चेहरा रोटी का चेहरा था.