 जिस तरह का सच यह है कि आईना झूठ नहीं बोलता, उसी तरह का सच यह भी है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता. इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि सच प्राकृतिक है; झूठ गढ़ना पड़ता है- फिर वह झूठ सौंदर्य प्रसाधनों से बोला जाए या खुराफाती-स्वार्थी इंसानी दिमाग से ! गोवा में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन, महोत्सव की जूरी के अध्यक्ष इस्राइली फिल्मकार नदव लापिद ने यही बात कही – न इससे कम कुछ, न इससे अधिक कुछ ! इसके बाद गर्हित राजनीति का जो वितंडा हमारे यहां फूट पड़ा, वह भी इसी सच को मजबूत करता है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे / झूठ की कोई इंतहा ही नहीं.
जिस तरह का सच यह है कि आईना झूठ नहीं बोलता, उसी तरह का सच यह भी है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता. इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि सच प्राकृतिक है; झूठ गढ़ना पड़ता है- फिर वह झूठ सौंदर्य प्रसाधनों से बोला जाए या खुराफाती-स्वार्थी इंसानी दिमाग से ! गोवा में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन, महोत्सव की जूरी के अध्यक्ष इस्राइली फिल्मकार नदव लापिद ने यही बात कही – न इससे कम कुछ, न इससे अधिक कुछ ! इसके बाद गर्हित राजनीति का जो वितंडा हमारे यहां फूट पड़ा, वह भी इसी सच को मजबूत करता है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे / झूठ की कोई इंतहा ही नहीं.
इतिहास बनाना इंसानी साहस की चरम उपलब्धि है; इतिहास को विकृत करना मानवीय विकृति का चरम है. हम दोनों ताकतों को एक साथ काम करते देखते हैं. इंसानी व सामाजिक जीवन में कला की एक अहम भूमिका यह भी है कि वह इन दोनों के फर्क को समझे व समझाए ! जो कला ऐसा नहीं कर पाती है वह कला नहीं, कूड़ा मात्र होती है. इसलिए कोई पिकासो ‘गुएर्निका’ रचता है, कोई चार्ली चैपलिन ‘द ग्रेट डिक्टेटर’ बनाता है, कोई एटनबरो ‘गांधी’ ले कर सामने आता है. अनगिनत पेंटिंगों, फिल्मों के बीच ये अपना अलग व अमर स्थान क्यों बना लेती हैं? इसलिए कि युद्ध की कुसंस्कृति को, विकृत मन की बारीकियों को तथा इंसानी संभावनाओं की असीमता को समझने में ये फिल्में हमारी मदद करती हैं. तो कला की एक सीधी परिभाषा यह बनती है कि जो मन को उन्मुक्त न करे, उद्दात्त न बनाए वह कला नहीं है.
दूसरी तरफ वे ताकतें भी काम करती हैं जो कला का कूड़ा बनाती रहती हैं ताकि सत्य व असत्य के बीच का, शुभ व अशुभ के बीच का, उद्दात्तता व मलिनता के बीच का फर्क इस तरह उजागर न हो जाए कि ये ताकतें बेपर्दा हो जाएं. विवेक की इसी नज़र से गोवा फिल्मोत्सव में बनी जूरी को 14 अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को देखना-जांचना था. लापिद इसी जूरी के अध्यक्ष थे. जूरी में या उसके अध्यक्ष के रूप में उनका चयन सही था या गलत, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए जिनका यह निर्णय था लेकिन 5 सदस्यों की जूरी अगर एक राय थी कि ‘कश्मीर फाइल्स’ किसी सम्मान की अधिकारी नहीं है, तो इस पर किसी भी स्तर पर, किसी भी तरह की आपत्ति उठना अनैतिक ही नहीं है, घटिया राजनीति है जिसका दौर अभी हमारे यहां चल रहा है.
लापिद ने जूरी के अध्यक्ष के रूप में महोत्सव के मंच से जब ‘कश्मीर फाइल्स’ को ‘अश्लील शोशेबाजी’ ( ‘वल्गर प्रोपगंडा’ का यह मेरा अनुवाद है) कहा तब वे कोई निजी टिप्पणी नहीं कर रहे थे, जूरी में बनी भावना को शब्द दे रहे थे. जूरी के बाकी तीनों विदेशी सदस्यों ने बयान दे कर लापिद का समर्थन किया है. भारतीय सदस्य सुदीप्तो सेन ने अब जो सफाई दी है वह बात को ज्यादा ही सही संदर्भ में रख देती है : “ यह सही बात है कि यह फिल्म हमने कला की कसौटी पर खारिज कर दी. लेकिन मेरी आपत्ति अध्यक्ष ने बयान पर है जो ‘कलात्मक’ नहीं था. ‘वल्गर’ व ‘प्रोपगंडा’ किसी भी तरह कलात्मक अभिव्यक्ति के शब्द नहीं हैं.” मतलब साफ है कि ‘कश्मीर फाइल्स’ कहीं से भी कला से सरोकार नहीं रखती है, इस बारे में जूरी एकमत थी. ऐसा क्यों था, इसकी सबसे गैर-राजनीतिक सफाई जो कोई भी अध्यक्ष दे सकता था, लापिद ने दी. उन्हें यह बताना ही चाहिए था कि क्यों जूरी ने उन्हें सौंपी गई 14 फिल्मों में से मात्र 13 फिल्मों में से ही अपना चयन किया, और 14वीं फिल्म को फिल्म ही नहीं माना ? जूरी के अध्यक्ष लापिद का धर्म था कि वे यह बताते. जिन शब्दों में लापिद ने वह बताया, वह कहीं से भी राजनीतिक, गलत, अशोभनीय या कला की भूमिका को कलंकित करने वाला नहीं था.
हमारे यहां ही कला-साहित्य-पत्रकारिता का आसमान इन दिनों इतना कायर व कलुषित हो गया है कि वहां कला व सच की जगह बची नहीं है. जूरी के विदेशी सदस्यों ने अपने बयान में इसे पहचाना है : “ हम लापिद के बयान के साथ खड़े हैं और यह साफ करना चाहते हैं कि हम इस फिल्म की विषयवस्तु के बारे में अपना कोई राजनीतिक नजरिया बताना नहीं चाहते हैं. हम केवल कला के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं और इसलिए महोत्सव के मंच का अपनी राजनीति के लिए व नविद पर निजी हमले के लिए जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हम दुखी हैं. हम जूरी का ऐसा कोई इरादा नहीं था.”
जब नविद से पूछा गया कि जिस फिल्म को जूरी ने किसी सम्मान के लायक नहीं माना, उस फिल्म पर आपको कोई टिप्पणी करनी ही क्यों चाहिए थी, नविद ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखी. यह कहने की जरूरत नहीं है कि ईमानदारी से खूबसूरत कलात्मक अभिव्यक्ति दूसरी नहीं होती है. नविद ने कहा : “ हां, आप ठीक कहते हैं, जूरी सामान्यत: ऐसा नहीं करती है. उनसे अपेक्षा यह होती है कि वे फिल्में देखें, उनका जायका लें, उनकी विशेषताओं का आकलन करें तथा विजेताओं का चयन करें. लेकिन तब यह बुनियादी सावधानी रखनी चाहिए थी कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्में महोत्सव के प्रतियोगता खंड में रखी ही न जाएं. दर्जनों महोत्सवों में मैं जूरी का हिस्सा रहा हूं, बर्लिन में भी, केंस में भी, लोकार्नो और वेनिस में भी. इनमें से कहीं भी, कभी भी मैंने ‘द कश्मीर फाइल्स ’ जैसी फिल्म नहीं देखी. जब आप जूरी पर ऐसी फिल्म देखने का बोझ डालते हैं, तब आपको ऐसी अभिव्यक्ति के लिए तैयार भी रहना चाहिए.”
सारा खेल तो यही था. यह सरकारी आदेश था या आयोजकों की स्वामी भक्ति का खुला प्रदर्शन था, यह तो वे ही जानें लेकिन चाल यह थी कि झांसे में एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सरकारी क्षद्म का यह चीथड़ा दिखा लिया जाए. जूरी मेजबानी के दवाब में आ कर अगर इसे सम्मानित कर दे, तो बटेर हाथ लगी; हाथ नहीं लगी तो दुनिया भर में हम अपना प्रचार दिखा गए, यह उपलब्धि तो हासिल होगी ही. नविद ने यह सारा खेल बिगाड़ दिया. इसलिए हमने देखा कि नविद को भारत स्थित इसराइल के राजदूत से गालियां दिलवाई गईं. जिन ‘अनुपम’ शब्दों में ‘ द कश्मीर फाइल्स’ गैंग ने नविद का शान-ए-मकदम किया, वह कला के चेहरे पर गर्हित राजनीति का कालिख मलना तो था ही, अंतरराष्ट्रीय कला बिरादरी में भारत को अपमानित करना भी था.
(05.12.2022)
मेरे ताजा लेखों के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ें
https://kumarprashantg.blogspot.com
![]()
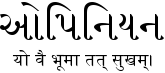

 सेवा वाली इला भी ऐसा ही एक नमूना थीं. गांधी ने सीधे उन्हें नहीं गढ़ा था, गांधी ने उन्हें छुआ था वैसे ही जैसे महानात्माएं हमें दूर से छूती हैं और गहरे आलोकित करती हैं. जहां तक मैं जानता हूं, 7 सितंबर 1933 को जनमी और 2 नवंबर 2022 को जिस इला भट्ट का अवसान हुआ, उन्हें कभी गांधी का सीधा साथ नहीं मिला और न वे गांधी आंदोलन में शरीक ही रहीं. होना संभव भी नहीं था. वकील पिता तथा महिलाओं के सवालों पर सक्रिय मां की बेटी इला तब 15 साल की थीं और स्कूलों-कॉलेजों की सीढ़ियां चढ़ रही थीं जब गांधी मारे गए. इसलिए उनके जीवन में गांधी को किसी पिछले दरवाजे से ही दाखिल होना था. वे उसी तरह दाखिल हुए भी. उनके साथ मिल-बैठ कर, बातें करते हुए मुझे सहज महसूस होता था कि यह गांधी की आभा से दीपित आत्मा है. वे छोटी कद-काठी की थीं, धीमी, मधुर आवाज में बोलती थीं जिसमें तैश नहीं, तरलता होती थी लेकिन आस्था की उनकी शक्ति न दबती थी, न छिपती थी. बहस नहीं करती थीं बल्कि बहसें उन तक पहुंच कर विराम पा जाती थीं क्योंकि आत्मप्रत्यय से प्राप्त एक अधिकार उनकी बातों में होता था. वे तर्कवानों की बातों की काट नहीं पेश करती थीं. काटना या तुर्की-ब-तुर्की जवाब देने जैसे हथियारों का वजन उठाना उनके व्यक्तित्व के साथ शोभता ही नहीं था लेकिन एक मजबूत इंकार की अभिव्यक्ति में वे चूकती भी नहीं थीं. सादगी की गरिमा और आत्मविश्वास का साहस उनमें कूट-कूट कर भरा था.
सेवा वाली इला भी ऐसा ही एक नमूना थीं. गांधी ने सीधे उन्हें नहीं गढ़ा था, गांधी ने उन्हें छुआ था वैसे ही जैसे महानात्माएं हमें दूर से छूती हैं और गहरे आलोकित करती हैं. जहां तक मैं जानता हूं, 7 सितंबर 1933 को जनमी और 2 नवंबर 2022 को जिस इला भट्ट का अवसान हुआ, उन्हें कभी गांधी का सीधा साथ नहीं मिला और न वे गांधी आंदोलन में शरीक ही रहीं. होना संभव भी नहीं था. वकील पिता तथा महिलाओं के सवालों पर सक्रिय मां की बेटी इला तब 15 साल की थीं और स्कूलों-कॉलेजों की सीढ़ियां चढ़ रही थीं जब गांधी मारे गए. इसलिए उनके जीवन में गांधी को किसी पिछले दरवाजे से ही दाखिल होना था. वे उसी तरह दाखिल हुए भी. उनके साथ मिल-बैठ कर, बातें करते हुए मुझे सहज महसूस होता था कि यह गांधी की आभा से दीपित आत्मा है. वे छोटी कद-काठी की थीं, धीमी, मधुर आवाज में बोलती थीं जिसमें तैश नहीं, तरलता होती थी लेकिन आस्था की उनकी शक्ति न दबती थी, न छिपती थी. बहस नहीं करती थीं बल्कि बहसें उन तक पहुंच कर विराम पा जाती थीं क्योंकि आत्मप्रत्यय से प्राप्त एक अधिकार उनकी बातों में होता था. वे तर्कवानों की बातों की काट नहीं पेश करती थीं. काटना या तुर्की-ब-तुर्की जवाब देने जैसे हथियारों का वजन उठाना उनके व्यक्तित्व के साथ शोभता ही नहीं था लेकिन एक मजबूत इंकार की अभिव्यक्ति में वे चूकती भी नहीं थीं. सादगी की गरिमा और आत्मविश्वास का साहस उनमें कूट-कूट कर भरा था. पहुंचे अहमदाबाद जहां एक मजदूर आंदोलन की खिंचड़ी पक रही थी. साराभाई-परिवार के कपड़ा मिलों का साम्राज्य तब बहुत बड़ा था. यहां के मजदूरों के संघर्ष की कमान गांधी ने संभाली. वह पूरी कहानी छोड़ कर इतना ही कि उस संघर्ष के गर्भ से पैदा हुआ मजूर-महाजन संगठन मजदूर आंदोलनों के इतिहास में गांधी की अपनी देन है. इला की ‘सेवा’ के पीछे मजूर-महाजन संगठन से मिला अनुभव था.
पहुंचे अहमदाबाद जहां एक मजदूर आंदोलन की खिंचड़ी पक रही थी. साराभाई-परिवार के कपड़ा मिलों का साम्राज्य तब बहुत बड़ा था. यहां के मजदूरों के संघर्ष की कमान गांधी ने संभाली. वह पूरी कहानी छोड़ कर इतना ही कि उस संघर्ष के गर्भ से पैदा हुआ मजूर-महाजन संगठन मजदूर आंदोलनों के इतिहास में गांधी की अपनी देन है. इला की ‘सेवा’ के पीछे मजूर-महाजन संगठन से मिला अनुभव था. सुनक एक प्रतिबद्ध, समर्पित ब्रितानी नागरिक हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए. उनका विवाह एक भारतीय लड़की से हुआ है. उस भारतीय लड़की का परिवार- नारायण-सुधामूर्ति परिवार- भारत के सबसे प्रतिष्ठित व संपन्न परिवारों में ऊंचा स्थान रखता है. इस लड़की से शादी के बाद सुनक इंग्लैंड के सबसे अमीर 250 लोगों में गिने जाते हैं. इसके अलावा सुनक का कोई तंतु भारत से नहीं जुड़ता है. न ऋषि सुनक भारत में जनमे हैं, न उनके माता-पिता, यशवीर व उषा सुनक का जन्म भारत में हुआ है. उनके दादा-दादी जरूर अविभाजित भारत के पंजाब के गुजरानवाला में पैदा हुए थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया. दादा-दादी परिवार ने भी अर्से पहले गुजरानवाला छोड़ दिया था और अफ्रीका जा बसे थे जहां से 1960 में, अर्द्ध-शताब्दी पहले वे इंग्लैंड जा बसे. जिस तरह अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा केन्या में जनमे थे और ईसाई धर्म में आस्था रखते हैं, ठीक वैसे ही सुनक इंग्लैंड में जनमे, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं. हमें अपनी सोनिया गांधी से सुनक को समझना चाहिए जिनका जन्म इटली में हुआ, जो जन्ममना ईसाई धर्म की अनुयायी हैं लेकिन एक भारतीय लड़के से शादी कर भारतीय बनीं तो आज उनका कोई भी तंतु इटली से पोषण नहीं पाता है. धर्म की परिकल्पना एक संकीर्ण बाड़े के रूप में करने वालों के लिए सोनिया व सुनक जैसे लोग एक उदाहरण बन जाते हैं कि धर्म निजी चयन व आस्था का विषय है, होना चाहिए लेकिन उससे नागरिकता या पहचान तय नहीं की जा सकती है. सुनक के मामले में ऐसा कर के हम इंग्लैंड के अंग्रेजों में मन में नाहक संकीर्णता का वह बीज बो देंगे जो कहीं है नहीं. यह न भारत के हित में है, न इंग्लैंड के.
सुनक एक प्रतिबद्ध, समर्पित ब्रितानी नागरिक हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए. उनका विवाह एक भारतीय लड़की से हुआ है. उस भारतीय लड़की का परिवार- नारायण-सुधामूर्ति परिवार- भारत के सबसे प्रतिष्ठित व संपन्न परिवारों में ऊंचा स्थान रखता है. इस लड़की से शादी के बाद सुनक इंग्लैंड के सबसे अमीर 250 लोगों में गिने जाते हैं. इसके अलावा सुनक का कोई तंतु भारत से नहीं जुड़ता है. न ऋषि सुनक भारत में जनमे हैं, न उनके माता-पिता, यशवीर व उषा सुनक का जन्म भारत में हुआ है. उनके दादा-दादी जरूर अविभाजित भारत के पंजाब के गुजरानवाला में पैदा हुए थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया. दादा-दादी परिवार ने भी अर्से पहले गुजरानवाला छोड़ दिया था और अफ्रीका जा बसे थे जहां से 1960 में, अर्द्ध-शताब्दी पहले वे इंग्लैंड जा बसे. जिस तरह अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा केन्या में जनमे थे और ईसाई धर्म में आस्था रखते हैं, ठीक वैसे ही सुनक इंग्लैंड में जनमे, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं. हमें अपनी सोनिया गांधी से सुनक को समझना चाहिए जिनका जन्म इटली में हुआ, जो जन्ममना ईसाई धर्म की अनुयायी हैं लेकिन एक भारतीय लड़के से शादी कर भारतीय बनीं तो आज उनका कोई भी तंतु इटली से पोषण नहीं पाता है. धर्म की परिकल्पना एक संकीर्ण बाड़े के रूप में करने वालों के लिए सोनिया व सुनक जैसे लोग एक उदाहरण बन जाते हैं कि धर्म निजी चयन व आस्था का विषय है, होना चाहिए लेकिन उससे नागरिकता या पहचान तय नहीं की जा सकती है. सुनक के मामले में ऐसा कर के हम इंग्लैंड के अंग्रेजों में मन में नाहक संकीर्णता का वह बीज बो देंगे जो कहीं है नहीं. यह न भारत के हित में है, न इंग्लैंड के.