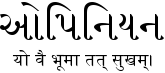આ સાથે મેં ભાઈ (મારા પિતાજી) વિષે થોડું લખ્યું છે તે મોકલું છું. એ મેં મારાં સંતાનો અને કુટુંબીજનો માટે જ લખ્યું છે, એટલે ઘણી કોશિશ કરવા છતાં જોઈએ તેવું ફોર્મલ નથી લખી શકી. એમની જન્મતિથિ 30મી ઓક્ટોબર છે, એટલે. … આખર આ એક એકાકી પુત્રીની એના માર્ગદર્શકને આપેલી અંજલિ છે.
− આશા બૂચ

नरेंद्रभाई अंजारिया
‘भाई’(मेरे पिताजी स्व. नरेंद्रभाई अंजारिया)का यह जन्मशताब्दीकी वर्ष. उनके गुणानुवाद यहाँ श्रद्धांजलिके रूपमें प्रस्तुत करना चाहूंगी।
नरेन्द्रभाईका जन्म ३० अक्टूबर १९२४, जामनगरमें हुआ था. पिता नौतमलाल अपनी पत्नी और पुत्रको परिवारजनोंकी छायामें छोड़ कर रोजगारकी तलाशमें 1927 पूर्व अफ्रिका गए. दो सालके बाद परिवार सहित टांगामें स्थायी रूपसे रहने लगे.
भाईके अफ्रीका निवास दरमियान एक बहन रंजन और एक भाई छोटुका जन्म हुआ. उनके भारत आने के बाद एक बहन मुद्रिकाका जन्म हुआ, जिन्हें जब वो नौ सालकी थी तब राजकोटमें पहेली दफा मिले। भाईकी प्राथमिक शिक्षाके श्री गणेश वहीं पर हुए.
भाई पांच साल अफ्रिकामें रहे. उसके बाद ई.स. १९३६में भाईके लिए राजकोटकी नागर बोर्डिंगमें रहेनेकी और आल्फ्रेड हाईस्कूलमें पढनेकी सुविधा करके माता-पिता अफ्रिका वापस गए. उस समयके नागर ज्ञातिके एक प्रतिष्ठित नेता उ.न. ढेबरको “अपने जैसा वकील बनाना’ ऐसी सिफारिश मेरे दादजीने की थी. सचमुच ढेबरभाईने भाईको ‘अपने जैसा’ बनाया, मगर वकील नहीं, बल्कि एक रचनात्मक कार्यकर!

स्थल : टांगा (सांप्रत समयके तंज़ानियाका एक छोटा गाँव) साल: १९२९
शाला और कॉलेजके अभ्यासकाल दौरान गाँधी विचारकी ज़ोरोंसे बहती हुई हवाने जवानीमें पांव रखते हुए भाईको भी आज़ादीकी लड़त और रचनात्मक कार्यकी ओर अपनी दिशा बदलनेके लिए आकर्षित किया. तत्वज्ञानके साथ बी.ऐ. के इम्तहाँमे अनुत्तरणीय होने के पीछे उनके अभ्यास करनेकी क्षमताके अभावसे बढ़कर आज़ादीके जंगमे जुड़ जानेका जोश और रचनात्मक कार्य करनेका उत्साह कारण स्वरूप होनेकी ज़्यादा संभावना रही होगी. आखिर उन्होंने बी.ऐ. की उपाधि हांसिल की और तुरंत ही राजकोटमें सौराष्ट्र रचनात्मक समिति द्वारा संचालित रचनात्मक कार्यको अपना कार्यक्षेत्र बना लिया. थोड़े समयके लिए स्व. ढेबरभाई और उस ज़मानेकी अग्रगण्य महिला प्रतिभा स्व. भक्तिबाके साथ रहेनेके मौक़ा मिला, जिसने भाईके जीवनको अनेक तरीकेसे समृद्ध बनाया. ई.स. १९५१से ‘५४ तक भाईने गुजरात विद्यापीठ – अहमदबादके हिंदी प्रचार केंद्रमें सेवा प्रदान की. ‘५४से लेकर ‘९६में अपने जीवनकी ज्योत बुझने तक हिंदी प्रचार और दूसरे अगण्य रचनात्मक कार्य करने वाले संगठनोंके ज़रिये मानद सेवा करते रहे. हिंदी प्रचारके कामसे जुड़े तभीसे भाईका रचनात्मक कार्यका दौर शुरू हुआ. विराणी कन्या विद्यालय और विराणी हाईस्कूलमें थोड़े समय तक शिक्षककी भूमिका निभाई. ‘अखिल भारत संस्था संघ’के सदस्य होने के पश्चात् सम्मेलनों, परिसंवादों और परिषदोंमें हिस्सा लेने हेतु पूरे भारतमें परिभ्रमण करनेका भाईको मौक़ा मिला.
यह हुआ भाईका संक्षिप्त जीवनवृत्त. आज मैं बात करना चाहती हूँ मेरे पिताजी मेरे मनसे दुसरे लोगोंसे क्यों भिन्न थे, उनमें क्या विशिष्ट गुण थे इसके बारमें.
‘भाई’ नामके उच्चारणके साथ ही एक सौम्य, शांत प्रतिभा नज़र समक्ष खड़ी हो जाती है. उनके तन और मनका स्वास्थ्य उनके गोल चहेरे, प्रेम बहाती हुई आँखें और सदा प्रसन्न हास्य मंडित मुखमुद्रामें प्रत्यक्ष होता रहता था. मितभाषी और
मृदुभाषी होना भी उनका जन्मदत्त स्वभाव था.

स्थल : टांगा (सांप्रत समयके तंज़ानियाका एक छोटा गाँव) साल : १९३५ शालाके पोशाकमें
भाईको लेकर मेरी याददाश्त पांच-छह सालकी उम्रसे शुरू हुई. मैंने भाईको सभी घरेलू कार्य करते हुए देखा था – खाना पकाने के सिवा! इसके पीछे स्त्री-पुरुषके बीच समानता साबित करनेका या तो खुद कुछ अलग विचारधाराका अनुसरण कर रहें हैं ऐसा दिखावा करनेका इरादा बिलकुल नहीं था, वह उनकी सहज प्रकृति थी. दिन जल्दी सुबहसे शुरू होता था और रातको भी पहले प्रहरकी नींद लेनेका नियमका अनुसरण करते थे. कितना भी काम क्यों न हो, भाईको कभी भी जल्दीसे निपटाते नहीं देखा, निर्धारित समय पर कार्य करनेके लिए कभी हाथमें लिया हुआ कार्य लपरवाहिसे करते हुए नहीं देखा। हरेक कार्य करनेमें दुरस्तीसे करनेका और व्यवस्था निभानेका आग्रह इतना था, मानों उन्होंने लश्करी या नर्सिंगकी तालीम न हांसिल की हो!
भाईने हम दोनों बहनोंकी हर तरहसे परवरिश की. हर कार्यमें भाई और बहन (मेरी माँ) हमेशा हमें अपने साथ रखते थे, इसलिए बहुत सारे काम उन्हें देखकर ही अपने आप सीख जाते थे, फिर भी वो हम पर नज़र रखते थे, कभी गलती हो जाय तो धीरे से बता देते थे, अगर कोई चूक हो जाय और महत्त्वकी बात हो तो नियमका पालन करनेके लिए दृढ़तासे कहते भी थे, मगर कभी ऊँची आवाज़से कुछ कहा हो ऐसा याद नहीं है. अन्य किसीकी गलतीसे नाराज़ हो जाय तब भाईका चहेरा लाल होते हुए ज़रूर देखा है.
हमारे परिवारमें जीवनके महत्वपूर्ण मूल्यों और मान्यताएं कैसे सीखे जाते हैं और अच्छे इंसान बनने के लिए ज़रूरी गुण कैसे आत्मसात कर सकते हैं यह सब बातों बातोंमे ही सिखने को मिल जाता था. ‘तू लकड़ी हो इसलिए ……. करना चाहिए या एक बेटी हो इसलिए ……. नहीं करना चाहिए’ ऐसा आदेश कभी नहीं सुना. दूसरोंके विचार, मंतव्य, उनके रुख़ और वयवहारको किस दृष्टिसे देखना चाहिए यह बात पर भाई बहुत ज़ोर देते थे, जिससे सबके साथ मेलजोलके संबंध स्थापित करके निभा सकते हैं ऐसा वो मानते थे. मुझे भाईकी यह बात आज भी बिलकुल याद है, “दूसरोंकी ७०% बात सिर्फ सुननेकी होती है, २५% बातके लिए अगर सामने वाला पूछे तो ही अपना मंतव्य दर्शानेकी ज़रूर होती है और सिर्फ ५% बातें ही ऐसी होती है जिसके बारेमें हमें कुछ मार्गदर्शन देनेकी ज़रूर होती है, और वो भी दे कर ‘हमें मुक्त हो जाना चाहिए’. मेरे मनसे यह उनका गीताका ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ बोधका व्यावहारिक अर्थघटन ही था. भाई एक दुसरे नियमके पालनका भी आग्रह रखते थे. जब विवादास्पद मुद्देकी चर्चा हो रही हो तो अपना मंतव्य उसी वख्त मत व्यक्त करो, क्योंकि उस वख्त आप मनसे विचलित हो गए होते हैं और अन्य लोग भी अपने दृष्टिकोण को सही साबित करनेका प्रयास करते है, उस समय एक दूसरेके स्वमानकी रक्षा न हो पाए ऐसा हो सकता है. अगर हो सके तो दूअसरोंकी बात शांतिसे सुननी चाहिए, उसके ऊपर अपनी और उनकी दृष्टिसे विचार करके थोड़े समयके बाद प्रतिभाव देना उचित रहता है. यह बहुत ही उपयोगी सूचन था. हालाँकि मैं उसका १००% पालन नहीं कर पाई हूँ यह मेरी कमी है. अपने निजी और व्यावसायिक जीवनमें इस नियमका यदि हम पालन करें तो ९०% संघर्ष पैदा ही न होते. भाईकी एक और भी विशिष्टता थी. वो हमारे या और किसी ऑरके (इसमें उनके कार्यक्षेत्रसे जुड़े हुए लोग भी शामिल थे) कुछ ख़रीदनेका, बाहर जानेका, छुट्टी लेनेका यातो कुछ कार्य करनेका प्रस्ताव सुनकर कभी भी तुरंत ‘हाँ’ या ‘ना’ कभी नहीं कहते. प्रस्ताव करने वाला थक जाये इतने सारे सवाल पूछकर सब जानकारी प्राप्त कर लेते, फिर खुद उसके ऊपर सोच विचार करके अपने हकारात्मक या नकारात्मक उत्तरके कारण बताते थे. इसका परिणाम यह हुआ करता था की, भले ही भाईका उत्तर हमारी इच्छाके मुताबिक़ न हो, मगर वह हमेशा हमारी भलाईके लिए है यह समजमें आनेसे इससे दुःख नहीं होता था. तत्वज्ञान और तर्कशास्त्रका अभ्यास करनेकी फलश्रुति स्वरूप ऐसी मनोदृष्टिका विकास हुआ होगा शायद. उसी तरह खाना खाते वक्त मन उद्विग्न हो ऐसी बातें, किसीकी निंदा करना या कोई नकारात्मक बातोंकी चर्चा न करनेका भाईका आग्रह था. जब छोटे थे तब हमने इस नियमका पालन किया, मगर जब अपना परिवार हुआ तो उसका मूल्य ज़्यादा समजमें आया. यह सब बातें छोटी मानी जा सकती हैं, मगर सबल और सरल व्यक्तित्व के विकासके लिए बहुत ही अहम मायना रखती है.
मेरा जन्म आज़ादी मिलनेके बाद तुरंत हुआ था. उन दिनों कई कन्याएं उच्च अभ्यास करने लगी थीं और महिलांए व्यवसाय भी करने लगीं थीं. महिलाओं के प्रति पुरुषोंका दृष्टिकोण भी बदलने लगा था,मगर मैंने यह भी निरीक्षण किया था कि आम जनताकी सेवामें संलग्न हों या अपनी ऊपरी अधिकारी हों ऐसी महिलाओंकी महत्ताका स्वीकार करने वाले ‘महानुभावों’ अपनी पत्नीको समानाधिकार या सम्मान, और वो भी अत्यंत सहज भावसे नहीं दे पाते थे. ऐसा क्यों होता होगा वह मुझे समझमें नहीं आता था. इसकी वजह यह थी कि भाई और बहनके संबंधमें मानव होना महत्व रखता था, नहीं की पति-पत्नीके पारंपरिक ख्यालात आधारित संबंध. इसी वजहसे बहन – मेरी माँ – शादीके बाद एस.एस.सी. से लेकर एम.ए. बी. एड. तक की शिक्षण यात्रा पूर्ण कर सकीं और उनकी सिध्धिका गौरव भाईकी सदा मुस्कुराती आंखोसे दिखाई देता था. मेरी और मेरी बहन स्मिताकी सिद्धिओं और सफलताओंसे भाईको ख़ुशी और गौरव ज़रूर महसूस होता था, मगर दूसरोंके सामने हमारी तारीफ करनेकी आदत नहीं रखते थे. इसीलिए हमें सफलता और असफलताको समभावसे समझनेकी आदत हो गई.
भाईके व्यक्तित्वका एक और गुण था, जो की दूसरोंमें छिपी हुई अच्छाई और ख़ास शक्तिको पहचानना. भाई हिंदी प्रचारके अलावा अनेक रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाओंके साथ जुड़े हुए थे इसलिए कार्यकर्ताओंकी क्षमता और उनकी कार्यपद्धतिओंमें वैविध्य अपरंपार था. किसी सहकार्यकरमें कोई कमी नज़रमें आये, तो उसे एकांतमें बुलाकर सुचना दे देते, मगर अन्यको इसकी भनक भी नहीं आती. इसी तरह अलग अलग मंतव्य और विचार वाले लोगोंकी बात अपार धैर्यसे सुनते और इससेभी अधिक धैर्यसे दोनों पक्षके लोगोंको एक दुसरे के दृष्टिकोण समजा कर समस्याका हल निकालनेकी कोशिश करते थे. इसी वजहसे मैंने कई लोगोंको अपनी समस्याओंका हल ढूँढ़नेके लिए भाईके पास आते हुए देखा था.
उस जमानेमें लोग मानते थे कि या तो खुद नेता बन जाओ या किसी नेताके पीछे पीछे चलने लगो. भाईमें वहीवटी कौशल्य, मुतसद्दीगिरिसे समस्याओंका हल निकलनेकी क्षमता और अपने कार्यक्षेत्रके प्रति संपूर्ण वफ़ादारीके गुण थे, फिरभी राजकीय महत्वाकांक्षा ना होनेकी वजहसे ‘नेता’ नहीं बने. और उपरोक्त सभी क्षमताएं होनेके कारण किसी नेताके अंध अनुयायी भी न बने. यही कारण है की किसीकी खुशामद करके खुदके या अपनी संस्थाके फायदेके लिए अपना स्वमान गिरवी रखते नहीं देखा. नेता दो प्रकारके होते हैं, एक, खुद आगे रहकर दूसरोंको अपना अनुसरण करनेका आदेश देते हैं, दुसरे प्रकारके लोग अन्य लोगोंके साथ चल कर उनको आगेकी राह दिखाते हैं. भाई दूसरे प्रकारके नेता थे. प्रसिध्धिसे योजनों दूर भागने वाले. पर्देके पीछे रहकर काम करने वाले. खुद दूसरों पर विश्वास करते थे और अपने हाथके नीचे काम करने वालोंको सक्षम बनाते थे. मूक सेवक किसे कहते हैं यह हमें इसी तरह समजमें आया.
वैसे तो भाई मितभाषी थे, मगर उनका मित्रोंका वर्तुल पूरी दुनियाको घेर सके इतना विशाल था. उसमें वैविध्य भी कितना! सौराष्ट्र और कच्छके छोटे से छोटे गांवके हिंदी प्रचारकसे ले कर दिल्ही, कलकत्ता, चेन्नईके प्रतिष्ठित संगठनोंके पदाधिकारिओं, कोंग्रेसके प्रमुख ढेबरभाई (हालांकि वो हमारे परिवारके बुज़ुर्ग सदस्य जैसे थे) और मोरारजी भाई देसाई तकके सबके नाम उनकी डायरीमें होते थे. इतना ही नहीं, उनके गांव या शहरमें भाईको अपने काम के सिलसिलेके बारेमें जाना होता था, तो उन लोगोंको अवश्य मिलने भी जाते! और वो लोग भी हमारे घर उनको मिलने आते! फिर भी भाईके मुँहसे “मैं इतने लोगोंको पहचानता हूँ, फलाने मंत्री या धारासभ्यके घर ठहरा था, फलाने लेखकने मुझे अपने घर बुलाया था” इसका ढोल पीटते नहीं सुना था. मित्रोंकी संख्यामें विदेशसे आये हुए विद्यार्थीगण और कर्मशीलोंभी शामिल हुए. वो सब हमारे परिवारका हिस्सा बन गए और आजीवन संपर्क रख कर संबंध निभाते रहे हैं, और वो भी न सिर्फ भाई और बहनके साथ मगर मेरे साथ और हमारे बच्चोंके साथ भी. ऐसी थी संबंधोंकी गहराई.
नम्रताकी एक और मिसाल. अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघने जब भाईका सम्मान किया था, तो उसकी खबर जब वे वहां पहुंचे तब हमें मिली. उन्होंने हमें एक पोस्टकार्ड लिखा, “इस सम्मेलनमें कुछ हिंदी प्रचारकोंका सम्मान होने वाला है, जिसमें गुजरातमेंसे मुझे पसंद किया गया है.” ऐसी प्रतिभाके धनि होनेसे भाईका शारीरिक कद नहीं बढ़ा, मगर उनका व्यक्तित्व महाकाय होता गया.
हिंदी प्रचारके कार्यको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला यह भी तो बताना चाहूंगी.

स्थान : नई दिल्ही साल: १९८९ – हिंदी प्रचार तथा हिंदी प्रशिक्षणके क्षेत्रमें महत्वका योगदान देने के लिए गंगाशरण सिंह पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधीके हाथ इनायत किया गया
उपरोक्त पुरस्कारके साथ मिली हुई धनराशि भाईने हिंदी समितिको समर्पित कर दी थी यह कहनेकी ज़रूरत नहीं है.
भाई शैक्षिणक उपाधियाँ हांसिल करनेमें समय व्यतीत करनेके बजाय समाजोपयोगी बुनियादी कार्योंको अपना जीवन मंत्र बना कर उसीमें निमग्न हो गए. उनका गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनो भाषाओँ पर अद्भुत प्रभुत्व. उर्दूभी पढ़ और लिख सकते थे, कोविदका प्रमाणपत्र मिला था उनको. सभी भाषाओंके उच्चारण अति विशुद्ध, और समझाते थे भी अत्यंत तन्मयताके साथ. जब वे १९१५मेँ प्रकाशित हुई भारतीय समाजमें विधवा महिलाओंकी अवदशाका वर्णन करती हुई ‘मुना जाते बेवा’ जैसी उर्दू और हिंदी मिश्रित कविता पढ़ते थे तो घंटो तक सुनने का मन करता था. भाई उत्तम शिक्षक तो थे ही, पर साथमें उनमें विचारोंकी स्पष्टता भी थी. खूब सोच विचार कर ही बोलते या लिखते. इसिलए उनके वक्तव्य संक्षिप्त, हर मुद्दे को स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत करने वाले और उनकी लिखाई विषयको न्याय देनेवाली रहा करती थी. लेख एक ही दफा लिख लेते, उसमें कोई सुधार करनेकी ज़रूरत नहीं रहती थी. अलग अलग विषयों पर लिखे २५से भी ज़्यादा लेख, ३०से भी ज़्यादा किताबोंका अनुवाद और करीब ३०-३५ रेडियो वार्तालापोंकी श्रृंखला भाईकी विचार और भाषा समृध्धिका व्याप सूचित करती है.
जन्मसे ले कर जीवनके अंत तकके सफरके दरमियान लोगोंके बाहरी दिखाव, निजी स्वभाव, बोल-चाल, व्यवहार और कार्यक्षेत्रसे प्राप्त पद और प्रतिष्ठामें कई बदलाव आते हुए हम सब देखते हैं. स्व. ढेबरभाईने भाईको सन १९२५में जब वे चार माहकी उम्रके थे तब देखा था और बीस साल बाद उन्हें देख कर पहचान गए और मेरे दादजीको लिखा, “कोई कृपालु शक्तीने उनकी कांतिको सम्हालके रखी है.” अफ्रिकामें आठ-दस सालके बालक नरेन्द्रको जिसने देखा था उनहोंने दशकोंके बाद भाई को पहचान लिया! किसीकी बाह्य प्रतिभामें भी इतना सातत्य बना रहे इसके पीछे अंतरकी निर्दोष भावना, प्रसन्नता और स्वभावकी सरलता ज़िम्मेवार होती होगी ऐसा मेरा मानना है.
सामान्यतया लोग तीन ‘प’ पानेके लिए ज़मीन आसमान एक करते हैं – पैसा, पद और प्रतिष्ठा. भाईको इन तीनोंमेसे एकभी ‘प’ पानेकी मनीषा नहीं थी, फिर भी एक से एक बढ़कर महत्वपूर्ण कार्य उनको ढूंढते हुए उनके पास आया करते थे, जिन्हें वो पर्देके पीछे रहकर निष्ठासे पूरा करते थे. कोई काम उनके मनसे छोटा नहीं था, इसलिए सभास्थल पर दरी बिछानी हो या उठा कर ठीक जगह पर रखनी हो, भाई वहाँ हाज़िर होते, किसी समितिका प्रस्ताव लिखना हो, कोई सम्मेलनमें मुख्य वक्ताकी हैसीयतसे प्रवचन देना हो, समान कुशलतासे काम करते. भाईके कार्यक्षेत्रका केंद्र भले ही हिंदी प्रचारका कार्य रहा हो, मगर बादमें उसमें हरिजनोद्धार, खादी-ग्रामोद्योग, प्रौढ़ शिक्षा, प्राणी कल्याण, यूनिवर्सिटीके सिंडिकेटका सभ्यपद और सर्वोदय तालीम जैसे अनेकविध रचनात्मक कार्यों जुड़ते गए. सभी कार्य अवेतन। इसीलिए ही ‘निष्काम कर्मयोगी’की उपाधि मिली.
यह हुई भाईके कार्यक्षेत्रकी एक झलक. परिवार, समाज और देश-दुनियाके बारेमें उनके विचार काफी उदार और परिपक्व थे. ‘सूखे दुखे समेकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ’ यह उपदेशात्मक अवतरण हमारे धार्मिक ग्रंथ, भजन और विद्वानोंके प्रवचनोंमे हमेशा सुनने मिलते हैं. उसका अमल करनेवाले ढूंढने पर भी नहीं मिलते. हमें घरमें ही मिल गए! मेरी छोटी बहन स्मिताकी आकस्मिक बिदा परिवारके लिए असह्य घाव था. भाई मौन हो गए, दैवकी मरज़ी स्वीकार करके दुखी होकर भी उस घाव को सहम कर झेल लिया. उनको पार्किंसन्सकी व्याधिका सामना करना पड़ा. मैंने पूछा, ‘आपको यह विचार नहीं सताता है की आप जैसे शुद्ध हृदयके इन्सानकी तकदीरमें ऐसी पीड़ा भुगतनेका क्यों लिखा?’ उत्तर दिया, “जिसका उत्तर न मिले उसके बारेमें सोच कर अस्वस्थ होने के बजाय ‘हमसे भी अधिक दुखी जन हैं’ यह सोचकर स्वस्थ रहकर कठिन परिस्थितिका उपाय करें, जिसका कोई उपाय न हो उसे सह लेनेमें ही समझदारी है.” मुझे वैष्णव जन और गीताके स्थितप्रग्नके लक्षण भाईके विचार-व्यवहारमें दिखाई देते थे.
भाईके बिदा होनेके बाद जो ‘स्मृति ग्रन्थ’ तैयार हुआ उसमें उनके साथी हिंदी प्रचारकगण, रचनात्मक कार्योंसे जुड़े हुए सहकार्यकारगण और कई स्नेही-संबंधीओंने ‘हिंदी प्रचारके जागृत प्रहरी’, ‘अनन्य सेवक’, राष्ट्रभाषाके उपासक’, अजातशत्रु’, ‘राष्ट्रभाषाके समर्पित पुजारी’, ‘साधुचरित’, ‘सत्वशील’ और ‘कोमल हृदयी’ आदि बहुत सरे विशेषण द्वारा भाईको श्रद्धांजलि अर्पित की. इतनी बड़ी तादादमें लोग भाईको सच्चे मायनेमें समझ सके उस बातका परम संतोष हुआ. साथमें यह पढ़कर मैंने सोचा, हमें तो इनके यह सब गुणोंका परिचय था ही. ‘मेरे भाई’ इतना कहूं तो इसमें यह सब समाविष्ट हो जाता है. उनके यह सब आयाम पारिवारिक संबंध और उनके वैविध्य सभर कार्यक्षेत्रमें किये हुए कार्योंमें सदा प्रत्यक्ष होनेका अनुभव किया है.
भाई और बहनके दिए हुए संस्कार और मूल्योंका दीप आजके तूफानी माहौलमें बुझ न जाये इसलिए हमारे जीवन रूप हाथोंका संरक्षण दे कर आनेवाली पीढीको यह सब सौंप देनेके लिए यथाशक्ति प्रयत्नशील रहते हैं. भाईकी प्रेम सभर ऑंखें और प्रसन्न मुख मुद्रा हमें हमेशा बल प्रदान करती रहेगी.
e.mail : 71abuch@gmail.com
![]()