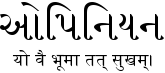कुमार प्रशांत
2026 में मैं अपनी बात 1948 से शुरू करूं, तो आप एतराज तो नहीं करेंगे ? मैं भी क्या करूं, अौर आप भी क्या करेंगे कि इतिहास इसी तरह हमारे साथ चलता है, और हम कहते हैं कि इतिहास स्वयं को दोहराता है !…
वह 27 जनवरी 1948 की सुबह थी. सांप्रदायिक हिंसा की अकल्पनीय आग में झुलसते, अपने खास साथियों के बदले तेवर से आहत, एकदम अकेले पड़ गए महात्मा गांधी बाजी पलटने की अपनी आखिरी कोशिश का नक्शा बनाने में लगे थे कि उस रोज सुप्रसिद्ध अमरीकी पत्रकार विन्सेंट शीन मुलाकात के लिए पहुंचे. गांधी के लिए शीन केवल पत्रकार होते तो उन्हें आज मिलने का वक्त न मिला होता, क्योंकि गांधी हर तरह की मुलाकात से तब इंकार कर रहे थे. शीन गांधी के आत्मीय अध्येता भी थे. इसलिए गांधी ने उन्हें बुला लिया था. लेकिन आज शीन गहरी उलझन में थे. उनका व्यथित मन कुछ सोच-समझ नहीं पा रहा था तभी वे गांधी तक पहुंचे थे. जिस दूसरे विश्वयुद्ध का शीन ने गांधी से अलग जा कर, जी-जान से समर्थन किया था, मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में ख़ुद को झोंक दिया था, उसकी असलियत अब सामने आ रही थी जो बेहद कुरूप व डरावनी थी.
“ लोकतंत्र को मजबूत बनाने के अच्छे उद्देश्य से जो विश्वयुद्ध लड़ा गया, उसका परिणाम इतना उल्टा क्यों आया ? एक हिटलर का मुकाबला करने जो लोग निकले थे, आज उनके भीतर से कितने ही छोटे-बड़े हिटलर पैदा हो गए हैं !” शीन का सवाल था.
“ सारा खेल साधनों का है !”, गांधी ने नि:शंक जवाब दिया, “ साध्य अच्छा हो, इतना काफी नहीं है, साधन शुद्ध हों, यह उससे भी ज्यादा जरूरी है. अशुद्ध साधन अच्छे साध्य को भी विकृत बना देते हैं.”
“ क्या हर स्थिति में, हर वक्त ऐसा ही होता है ?”
“ हमेशा ऐसा ही होता है, होगा; क्योंकि सत्य बदलता नहीं है.”
यह 1948 की दिल्ली थी; आज हम 2026 के दावोस में हैं. दोनों के बीच सिर्फ 78 साल का फासला नहीं है बल्कि यह भी है कि आज हमारे बीच कोई गांधी नहीं हैं. हम यहां गांधी को नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को सुन रहे हैं. वे दावोस के वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम में कह रहे हैं कि महाशक्तियों के वर्चस्व के खिलाफ हम ‘दोयम शक्तियों’को इकट्ठा होना होगा. वे कह रहे हैं कि अमरीकी साम्राज्यवादी शक्तियों का मुकाबला करने की सशस्त्र ताकत नहीं होगी हमारी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे : “ वह देश जिसके पास अपनी ज़रूरत का खाना नहीं है, जिसके पास अपनी जरूरत की ऊर्जा नहीं है, जो अपनी रक्षा में स्वंय समर्थ नहीं है, उसके लिए आज की दुनिया में ज्यादा कुछ विकल्प है नहीं. जब अंतरराष्ट्रीय विधि-विधान आपका संरक्षण नहीं कर सकते तब आपको अपना संरक्षण स्वयं करना होता है.”
यह संभवतः: पहला ही अवसर था जब नाटो के मंच से, किसी यूरोपीय देश ने अमरीका का नाम ले कर, उसके वर्चस्व को ललकारा ही नहीं बल्कि उससे छूटने के लिए नाटो देशों के साथ आने की बात कही. स्वाभाविक ही था कि डोनल्ड ट्रंप कार्नी से खार खाए बैठे हैं और चीख रहे हैं कि अमरीका के बिना कनाडा एक बड़ा जीरो है जिसे हम उसकी औकात बता देंगे ! यह अंतरराष्ट्रीय संवाद की नई भाषा है. हम भारतीय तो 2014 से ही ऐसी भाषा के आदी हो गए हैं.
आगे चलने से पहले हम इतिहास का एक दूसरा पन्ना भी पलटते चलते हैं. तब दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त हुआ था. तथाकथित मित्र-राष्ट्रों ने विजेता की भूमिका में दुनिया की कुंडली लिखनी शुरू कर दी थी. वे देशों के मनमाना विभाजन किए जा रहे था, अरबों की धरती पर बंदूक का हल चला कर इसराइल की खेती की जा रही थी. ऐसे वक्त में जवाहरलाल नेहरू नाम का एक आदमी सामने आया. उसने कहा था कि हम महाशक्तियों के इस खेल में किसी की तरफ नहीं हैं. हमारा रास्ता तीसरा है. तटस्थ राष्ट्रों का हम अपना संगठन बनाएंगे. महाशक्तियों के निर्दयी अंतरराष्ट्रीय खेल के बीच यह परम साहस की सोच थी, अंधेरे में लगाई एक वीरतापूर्ण छलांग थी. कोई जवाहरलाल ही ऐसी पहल कर सकता था, क्योंकि उसने गांधी की छाया में सांस ली थी.
नेहरू के आवाज उठाई तो साथ आ जुड़े इंडोनेशिया के सुकार्णों, मिस्र के गमाल नासेर. फिर तो यह बात रफ़्तार पकड़ गई और एक वक्त 120 देश इसमें शामिल हुए. यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो भी साथ आ खड़े हुए. रूसी व अमरीकी खेमा कौतुक से इस नई शक्ति के उदय को देखता रहा. जवाहरलाल ने 120 देशों की तरफ से कहा कि हम वे हैं जो अपना रास्ता ख़ुद बनाते हैं. लेकिन यह साहसी पहल धीरे-धीरे बिखरने लगी, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीतिक तटस्थता का नहीं था, सवाल तो शक्ति की पूरी अवधारणा का था. शक्ति की अवधारणा वैसी ही हो जैसी महाशक्तियों की है, तब तटस्थता सधती नहीं है. साध्य व साधन के विवेक की जो बात गांधी शीन को समझा रहे थे, जवाहरलाल न उसे समझ सके, न समझा सके. आज तटस्थ राष्ट्रों की वह सारी परिकल्पना ढह चुकी है, तो इसलिए कि तटस्थ राष्ट्रों के मानक भी महाशक्तियों जैसे ही थे. इसलिए हम यह शोकांतिका भी देखते हैं कि तटस्थ राष्ट्रों के मलबे में से एक-के-बाद एक तानाशाह या एकाधिकारी शासक उभर आए. नासेर, सुकार्णो, एंक्रूमा, टीटो अादि सबने सत्ता अपनी जेब में रखी ली. अपवाद रहे केवल जवाहरलाल जो तटस्थ कितने रहे यह विवाद का विषय है लेकिन लोकतंत्र को सीने से लगाए रहे, इसकी गवाही इतिहास भी देता है.
मार्क कार्नी क्या यह समझ पाते हैं कि तटस्थता का यह पूरा भव्य दर्शन क्यों विफल हुआ ? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि जवाहरलाल समेत सारे तटस्थ नेताओं की आंखों में सपना तो यही था कि हम अमरीका या रूस जैसे कैसे बनें. जवाहरलाल अपने भारत के लिए अमरीका-रूस की एक विचित्र-सी खिंचड़ी बनाने में व्यस्त थे. यहां भी हाल वैसा ही है. कार्नी के कनाडा समेत नाटो के सभी देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आज तक अमरीकी त्रिशूल भांजते चले हैं. अमरीका से ज्यादा अमरीकी बनने की होड़ में इन देशों ने वह सब किया जो अमरीका ने चाहा. वे लुटेरी अमरीकी राजनीति के सिपाही बने रहे, लूट में हिस्सेदारी करते रहे. कनाडा तो जी-7 के उस क्लब का सदस्य रहा जो सारी दुनिया में पूंजी के बल पर अट्टहास करता रहा है. यह बात अलग है कि आका जितनी छूट देता था, इन्हें उतने से ही संतोष करना होता था. जंगल का एक सच यह है कि शेर अपना शिकार खा कर जो बचा-खुचा छोड़ देता है, भेड़िए और सियार उसका भोग लगाते हैं. इसलिए कार्नी ने यह नहीं कहा कि ‘मध्यम शक्तियों’ को शक्ति की नई परिभाषा बनानी होगी तथा उसका राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पालन भी करना होगा. कार्नी ने यह नहीं कहा कि सारा यूरोप अमरीका का उच्छिष्ठ खाता रहा है. उन्होंने दुख भरे शब्दों में यह जरूर कहा कि हम ‘मध्यम शक्ति’ वालों ने गलत क्या-क्या किया लेकिन यह नहीं कहा उन गलतियों से बचने के लिए अब कनाडा क्या-क्या अलग करेगा ? हम देख ही तो रहे हैं कि उसी ट्रंप की कृपादृष्टि पाने की कोशिशें आज भी चल रही हैं.
बोर्ड ऑफ पीस का जो नया पासा ट्रंप महाशय ने फेंका है, उसे लपकने वालों की कमी नहीं है. यह नया नाटो है, यह नया संयुक्त राष्ट्रसंघ बनाने की चालाकी है इस सावधानी के साथ कि अब कोई अमरीकी सत्ता को ( ट्रंप को !) आंख न दिखा सके. इसलिए ट्रंप ने घोषणा की है कि बोर्ड ऑफ पीस का अध्यक्ष अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, डोनल्ड ट्रंप हैं जिन्हें कोई हटा नहीं सकता है. उन्होंने यह भी बता दिया है कि आज जो भी इस बोर्ड की सदस्यता लेंगे वे केवल 3 सालों के लिए सदस्य रहेंगे. स्थायी सदस्यता उन्हें ही मिलेगी जो सदस्यता के पहले वर्ष में ही अमरीकी खजाने में 1 बीलियन डॉलर की फीस नकद भरेंगे. जिस बोर्ड ऑफ पीस की आधी-अधूरी परिकल्पना ट्रंप महाशय ने सिर्फ गजा के संदर्भ रखी थी, अब सारी दुनिया उसके दायरे में आ गई है. जब ट्रंप का दावा सारी दुनिया में युद्ध रुकवाने का है तो वे उसकी कीमत सारी दुनिया की स्वायत्तता को अपनी मुट्ठी में कर के क्यों न वसूलें !
भारत ने तो देश-दुनिया के उन सारे सवालों के बारे में मौन धार लिया है जिनके बारे में कोई नैतिक भूमिका न लें आप तो उसे राजनीतिक चातुरी नहीं, राजनीतिक कायरता या अवसरवादिता कहते हैं. इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आज भारत की कोई हैसियत नहीं है याकि जैसा ट्रंप बार-बार साबित करते रहते हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय विदूषक भर रह गया है.
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से दुनिया की जो बंदरबांट चली है, उसका आधार रूसी व अमरीकी गुटों का निहित स्वार्थ रहा है. अब रूसी गुट जैसा कुछ बचा नहीं है. इधर के दिनों में रूस-चीन गुट-सा जो दिखाई देता है, वह अमरीकी गुट से डरे पुतिन-जिनपिंग की चालबाजी भर है. जो एक-दूसरे से भयभीत हों, जैसे उनकी साझेदारी संभव नहीं है वैसे ही जिनका एक-दूसरे पर रत्ती भर भरोसा न हो, उनकी साझेदारी भी संभव नहीं है. चोरों की साझेदारी भी इसलिए निभती है कि वे एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं.
ले-दे कर बच रहा था अमरीकी खेमा जिसके साथ नाटो था, पाकिस्तान भी जिसे नमस्कार करता था, हिंदुस्तान तो घुटनों पर ही था, इसराइल तथा ऐसे ही दूसरे मुल्क भी थे जिन्हें अॉक्सीजन के लिए अमरीका की तरफ देखना पड़ता था. ट्रंप ने इन सबमें पलीता लगा दिया. यह पागलपन नहीं है. ‘अमेरिका फर्स्ट’ का शंखनाद हो कि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का उद्घोष हो ( विश्वगुरू !), दोनों कहते यही हैं कि दुनिया में दूसरा कोई भी ऐसा न बचे कि जिसकी गर्दन तनी रहे. इसलिए ट्रंप हैं, इसलिए अमरीका है.
हम ऐसे अमेरिका के सामने हैं, अौर हमें उसके साथ अपना रिश्ता सुनिश्चित करना है. नरेंद्र मोदी के भारत ने तय किया था कि ट्रंप के कंधों पर बैठ कर भारत को बड़ा दीखना है. वह सारी फूहड़ डिप्लोमेसी आज सड़क किनारे धूल खाती पड़ी है, क्योंकि ट्रंप जैसों को अपने कंधों की बराबरी का कोई देश नहीं चाहिए. इसलिए कार्नी हों कि मैक्रोंन कि खुमैनी कि दूसरे कोई, हर किसी को अंतिम तौर पर समझ लेना चाहिए कि छोटा अमेरिका बनने की हसरत न पालें, क्योंकि बड़े ट्रंप साहब को ऐसी बराबरी सख्त नापसंद है.
कार्नी ‘मध्यम शक्ति’ की जिस नई भूमिका की बात करते हैं वह अपना रास्ता गढ़ने की बात है. लेकिन इसमें एक पेंच है. अपना रास्ता दूसरों को दबा या कुचल कर न बनाया जा सकता है, न उस पर चला जा सकता है. अपनी पसंद का रास्ता बनाने व उस पर चलने की कीमत अदा करनी पड़ती है जिसे गांधी ‘साधन की शुद्धता’ कहते हैं. जो साधन की शुद्धता की कीमत अदा करने को तैयार नहीं होते हैं उन्हें ट्रंप के अंगूठे के नीचे जीने की आदत बना लेनी चाहिए.
(27.01.2026)
मेरे ताजा लेखों के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ें
https://kumarprashantg.blogspot.com
![]()